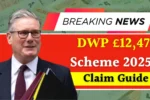आज के समय में जब जमीन की उपज शक्ति कम हो रही है और रासायनिक खादों का असर घटता जा रहा है, ऐसे में कार्बनिक खाद (Organic Fertiliser) किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। ग्रामीण भारत में खेतों में बचने वाला कचरा, जैसे डंठल, सूखी घास और पत्तियां, अब बेकार नहीं बल्कि ‘खजाना’ बन गए हैं। सरकार ने भी किसानों को जैविक खेती की दिशा में बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे।
कई राज्यों में किसान अब अपने खेतों के अवशेष को जलाने की बजाय उनसे कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे हैं। इससे प्रदूषण भी नहीं होता और खेतों को प्राकृतिक पोषण भी मिलता है। कार्बनिक खाद तैयार करने में ज्यादा खर्च नहीं आता और यह किसी भी मिट्टी में प्रयोग की जा सकती है।
जैविक खाद को अपनाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को सक्रिय रखती है और लंबे समय तक उपज क्षमता बनाए रखती है। यही वजह है कि भारत सरकार ने ‘गोबर-धन योजना’ और ‘पराली प्रबंधन अभियान’ जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो इस दिशा में बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं।
Organic Fertiliser 2025
कार्बनिक खाद (Organic Fertiliser) वह पदार्थ है जो प्राकृतिक स्रोतों से बनता है, जैसे गोबर, पत्तियां, पराली, फसल अवशेष, बची हुई सब्जियां, फलों के छिलके, और जैविक कचरा। इन सामग्रियों को सड़ने और गलने दिया जाता है जिससे पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम उत्पन्न होते हैं। यह खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ उसकी संरचना में भी सुधार करती है।
रासायनिक खाद की तुलना में कार्बनिक खाद बनाने में समय ज्यादा लगता है, पर इसका असर लंबे समय तक रहता है। जहां रासायनिक खाद केवल फसल पर तेज असर देती है, वहीं जैविक खाद मिट्टी की सेहत को स्थायी रूप से बेहतर बनाती है।
खेत के डंठल और घास से बनेगी सोने जैसी खाद
फसल कटाई के बाद खेत में बड़ी मात्रा में डंठल और सूखी घास बच जाती है। पहले किसान इसे जला देते थे, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता था और जमीन की ऊपरी परत की गुणवत्ता नष्ट हो जाती थी। अब यही कचरा जैविक खाद का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है।
किसान इन डंठलों को इकठ्ठा कर एक गड्ढे में डालते हैं और उस पर थोड़ा-सा पानी और गोबर डालकर ढक देते हैं। करीब 30 से 45 दिनों में यह पूरा मिश्रण सड़कर काली, महीन और पौष्टिक खाद बन जाता है। इस खाद को खेतों में डालने से फसल की जड़ मजबूत होती है और उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है।
कई कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हर किसान जैविक खाद तैयार करे तो खेतों की मिट्टी को फिर से जीवंत किया जा सकता है। इससे रासायनिक खाद की निर्भरता घटेगी और खेती की लागत भी कम होगी।
सरकार की पहल: गोबर-धन योजना और पराली प्रबंधन योजना
भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक कचरे को धन में बदलने के लिए गोबर-धन योजना (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) शुरू की है। इस योजना के तहत गांवों में गोबर और जैविक अपशिष्ट से बायोगैस और जैविक खाद बनाने की व्यवस्था की जा रही है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसान और ग्राम पंचायतें मिलकर गोबर और अन्य जैविक कचरे को खाद या ऊर्जा स्रोत में बदलें। केंद्र व राज्य सरकारें इसके लिए वित्तीय सहायता भी देती हैं। ग्रामीण स्तर पर बायोगैस प्लांट लगाने और कंपोस्ट यूनिटों की स्थापना के लिए अनुदान उपलब्ध है।
दूसरी ओर, पराली प्रबंधन योजना किसानों को पराली (फसल के अवशेष) जलाने से रोकने पर केंद्रित है। इसके तहत उन्हें मशीनें, जैसे हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम और बायो-डीकंपोजर, रियायती दरों पर दी जाती हैं। बायो-डीकंपोजर खेत में डालने से पराली कुछ ही दिनों में सड़कर उर्वर खाद में बदल जाती है।
कार्बनिक खाद तैयार करने की प्रक्रिया
कार्बनिक खाद तैयार करने के लिए किसानों को ज्यादा तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं होती। इसे घरेलू स्तर से लेकर खेत के पैमाने पर तैयार किया जा सकता है।
- सबसे पहले खेत से बचा कचरा, पत्ते, डंठल, सब्जियों के अवशेष आदि इकट्ठा करें।
- इन सब चीजों को एक गड्ढे या खुले ड्रम में डालें।
- हर परत पर पानी और गोबर या छाछ का मिश्रण डालें ताकि यह जल्दी सड़ सके।
- ऊपर से सूखी मिट्टी डालकर ढक दें और 30-40 दिनों तक इसे सड़ने दें।
- तैयार खाद काली और बिना बदबू वाली होगी, जिसे खेत में सीधे प्रयोग किया जा सकता है।
यह प्रक्रिया बेहद कम खर्चीली है और किसान अपने खेत में ही इसे तैयार कर सकते हैं।
सरकार और किसानों के लिए फायदे
इस योजना से किसानों की खेती की लागत घटती है क्योंकि उन्हें बाजार से महंगी यूरिया या डीएपी खाद खरीदनी नहीं पड़ती। मिट्टी में जैविक सामग्री बढ़ने से उसकी जल धारण क्षमता भी सुधरती है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है।
सरकार के स्तर पर भी यह योजना बड़ा पर्यावरणीय लाभ देती है। पराली जलाने की समस्या घटने से प्रदूषण कम होता है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं क्योंकि जैविक खाद और बायोगैस दोनों का बाजार मूल्य है।
किसानों के लिए अतिरिक्त लाभ और मदद
केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी इस दिशा में किसानों को प्रोत्साहित कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर, हरियाणा और पंजाब में किसानों को पराली प्रबंधन उपकरणों पर 50 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों को कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए फंड दिए जा रहे हैं।
किसान अगर अपने खेत में गोबर या जैविक कंपोस्ट यूनिट लगाते हैं तो उन्हें कृषि विभाग की ओर से किसान प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता मिलती है। कई जगह कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) किसानों को मुफ्त में जैविक खाद तैयार करने की विधि सिखा रहे हैं ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सकें।
निष्कर्ष
खेतों का कचरा यदि सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो यह न केवल खेत की सेहत सुधार सकता है बल्कि किसान की आमदनी भी बढ़ा सकता है। सरकार की योजनाओं का उद्देश्य यही है कि किसान रासायनिक खाद पर निर्भर न रहें और अपने खेतों को प्राकृतिक तरीके से उपजाऊ बनाएं।